इतिहास
बपतिस्मा और नमाज़ की पद्धति यहूदी, ईसाई और इस्लाम ने क्या मांडेवाद और पारसी धर्म से ली?

‘राजा मनु और जल प्रलय’ की कहानी जिस तरह ‘हज़रत नूह की नौका’ के नाम से जानी जाती है, उसी तरह क्या बपतिस्मा और नमाज़ का रस्मो-रिवाज़ (पद्धति) भी यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों ने मांडेवाद और पारसी धर्म से लिया, यह एक ऐसा सवाल है, जो बौद्धिक जगत में अक्सर चर्चा का विषय रहता है.कहा जाता है कि बपतिस्मा और नमाज़ का चलन काफ़ी पहले से था, जिन्हें बाद में अस्तित्व में आए इब्राहिमी पंथों/मज़हब ने भी कुछ बदलाव के साथ उनके नाम बदलकर अपना लिया था.आख़िर, सच क्या है?
मानव जाति और धर्म के इतिहास से जुड़े कई ऐसे पहलू हैं, जो आज भी सवाल बनकर खड़े हैं.उन्हीं सवालों में एक सवाल रीति-रिवाजों और नियमों को लेकर है.एक जाति में पाई जाने वाली रस्में दूसरी जाति/जातियों से क्यों मिलती हैं, इसका पता लगाने के लिए अध्ययन एवं चिंतन की ज़रूरत है.इसी प्रकार, इब्राहिमी अथवा पैगंबरी मज़हब कहलाने वाले यहूदी, ईसाइयत और इस्लाम में बपतिस्मा और नमाज़ के विधान अथवा संस्कार मांडियन और जोरास्ट्रियन से क्यों मिलते-जुलते हैं, यह सवाल ठीक वैसा ही सवाल है, जिसमें अक्सर ये पूछा जाता है कि क्या बाद में अस्तित्व में आए मज़हब-पंथों ने पहले से स्थापित धर्म/मज़हब में चली आ रही उपासना-पद्धति को ही अपनी भाषा-शैली में अपना लिया था.ज़वाब भी मिलते-जुलते ही होंगें, मगर, क्या? किसी निर्णय तक पहुंचने से पहले उपरोक्त रिवाज-संस्कारों के इतिहास को खंगालना होगा और कालांतर में उनके स्वरुप और चलन से जुड़े तथ्यों की गहन समीक्षा करनी होगी.
बपतिस्मा की पद्धति
ग्रीक शब्द बेप्टिजो से निकला बैप्टिज्म यानि बपतिस्मा का मतलब प्रक्षालन यानि डुबोना होता है.मूल रूप में, यह शुद्दिकरण के उद्देश्य से किया जाने वाला एक तरह का धार्मिक स्नान होता है, जो विभिन्न पैगंबरवादी मजहबों में अलग-अलग रूप में और अलग-अलग नाम से सदियों से प्रचलन में है.ईसाई इसे बैप्टिज्म यानि बप्तिस्मा कहते हैं और यहूदी मिकवाह, जबकि मांडियन लोगों में यह मस्बुता के नाम से जाना जाता है.माना जाता है कि बपतिस्मा की रस्म की शुरुआत मांडियन लोगों ने ही की थी, जिसे बाद में यहूदियों और फिर ईसाइयों ने भी अपना लिया.
मांडियन और बपतिस्मा
मांडियन अथवा सबियन एक अद्वैतवादी और रहस्यवादी पैगंबरी मज़हब मांडेवाद (Mandaeism), जिसे सब्यवाद (Sabianism) भी कहा जाता है, को मानने वाले लोग हैं.कई देशों में फैले क़रीब एक लाख से भी कम की संख्या में बचे इन लोगों की उपासना पद्धति का अस्तित्व यहूदियों से भी पुराना समझा जाता है.दक्षिण-पूर्व मेसोपोटामियन अरामीक भाषा मांडिक (Mandaic) में लिखित इनकी विभिन्न धार्मिक पुस्तकों में गिंज़ा रब्बा, हरन गवैता आदि प्रमुख हैं.गिंज़ा रब्बा इतिहास, धर्मशास्त्र और प्रार्थनाओं का संग्रह है.इनमें मस्बुता यानि बपतिस्मा को एक कर्मकांड के रूप में बताया गया है, जो आत्मा को मोक्ष के क़रीब ले जाने में सक्षम है.
धर्मांतरण की मानसिकता से कोसों दूर और आत्मरक्षा के लिए भी हिंसा से परहेज़ करने वाले मांडियन के लिए बपतिस्मा दूसरे मज़हब की तरह एक बार या कभी-कभार की रस्म नहीं, बल्कि यह बार-बार करने की ज़रूरी क्रिया है.इसलिए ये लोग हर रविवार (अपने पवित्र दिन) बपतिस्मा की रस्म के रूप में बहते हुए पानी में डुबकी लगाते हैं/पूर्ण विसर्जन/निमज्जन करते हैं.
नियम के अनुसार, मांडियन लोगों के ‘मासीकटा’ नामक ‘आत्मा आरोहण समारोह’ के पवित्र तेल और रोटी-पानी के भोज में शामिल होने से पहले मस्बुता ज़रूरी होता है.
महिलाओं के मासिक धर्म या प्रसव के बाद, पुरुषों और महिलाओं द्वारा यौन क्रिया या रात के उत्सर्जन के बाद, मृत शरीर के संपर्क में आने या फिर किसी भी दूसरी तरह की शारीरिक अशुद्धि की अवस्था में भी मस्बुता का विधान है.
मांडियन बपतिस्मा संबंधी रस्मो-रिवाज़ के लिए उपयुक्त एवं पवित्र मानी जाने वाली सभी नदियों को यर्डाना/यर्दन (जॉर्डन) कहते हैं.बाइबल में जकरिया और एलिज़ाबेथ के पुत्र बपतिस्मा-दाता युहन्ना अथवा जॉन द बैप्टिस्ट (John the Baptist) द्वारा यर्दन नदी में ही लोगों को बपतिस्मा दिए जाने का उल्लेख है.बाइबल के अनुसार, यीशु को युहन्ना ने ही बपतिस्मा दिया था.
उल्लेखनीय है कि आदम, उनके बेटे हबील और सेथ, उनके पोते एनोश के साथ-साथ नूह, शेम और राम/अराम को पैगंबर/नबी के रूप में अपना प्रत्यक्ष पूर्वज मानने वाले मांडियन अब्राहम, मूसा और यीशु को अपने धर्म का अनुयायी तो मानते हैं, लेकिन उन्हें भटका हुआ और झूठा बताते हुए उनसे नफ़रत करते हैं, जबकि युहन्ना अथवा जॉन को बहुत ऊंचा स्थान देते हैं, सम्मान करते हैं.यही कारण है कि कुछ विद्वान इन्हें (मांडियन को) ‘सेंट जॉन के ईसाई’ भी कहते हैं.
जैतून की दो लकड़ियों से बना क्रॉस की आकृति का एक बैनर द्राब्शा या दरफ़श, जो शुद्ध सफ़ेद रेशम के कपड़े के टुकड़े और मेहंदी की सात शाखाओं से ढंका होता है, मांडियन की आस्था का प्रतीक होता है.मगर महत्वपूर्ण बात ये है कि इस पारंपरिक दरफ़श का ईसाई क्रॉस यानि ईसा मसीह के सलीब से कोई संबंध नहीं है.
कुछ विद्वानों के अनुसार, दुनियाभर में और ख़ासतौर से भारत भ्रमण करने वाले मांडियन शायद तत्कालीन विश्वप्रसिद्ध ज्ञान का केंद्र रहे नालंदा पहुंचे होंगें और यहीं उन्हें गिंज़ा रब्बा, तौरात, इंजील, बाइबल और कुरान से बहुत पहले लिखे गए मत्स्य पुराण में वर्णित राजर्षि सत्यव्रत (वैवस्वत मनु) और जल प्रलय की कथा की जानकारी मिली होगी, और तभी मनु अलग भाषा-शैली में नूह बन गए और ‘नूह की नौका’ नामक कहानी मांडव्यवाद से होती हुई यहूदी, ईसाई और इस्लाम में भी दाख़िल हो गई.इसी क्रम में में, मांडियन यात्रियों को सनातन हिन्दू धर्म में प्रचलित नदियों के जल (ख़ासतौर से गंगाजल) से स्नान के द्वारा पाप धोकर पवित्र होने/मोक्ष प्राप्त करने की अवधारणा भी मिली होगी, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने मस्बुता नामक अपनी सबसे ख़ास रस्म की शुरुआत की, जिसे बाद में यहूदी और ईसाइयों ने भी मिकवाह तथा बपतिस्मा के नाम से इसे अपना लिया.
बहरहाल, मांडियन जॉन द बैप्टिस्ट/युहन्ना की बहुत इज्ज़त करते हैं, उन्हें अपना आख़िरी गुरु/नबी मानते हैं.क़रीब 1290 के दौर में, टस्कनी के एक डोमिनिकन कैथोलिक रिकोल्डो द मोंटेक्रोस अथवा रिकोल्डो पेनिनी जब मेसोपोटामिया में था, वहां उसकी मुलाक़ात कुछ मांडियन लोगों से हुई थी.उसने उनका ज़िक्र इस तरह किया-
” बग़दाद के पास रेगिस्तान में रहने वाले बहुत ही अज़ीब और विलक्षण लोग, जो सेबियन कहलाते हैं, मेरे पास आए और गुज़ारिश की कि मैं उनके यहां उनसे जाकर मिलूं.वे बहुत ही सीधे-सादे लोग हैं और ये दावा करते हैं कि उनके पास उपरवाले का दिया एक गुप्त नियम है, जिसे वे ख़ूबसूरत किताबों में बड़ी हिफाज़त से रखते हैं.उनका लेखन सीरिएक और अरबी के बीच एक तरह का मध्य मार्ग है.
वे ख़तने की वज़ह से इब्राहीम से नफ़रत करते हैं, जबकि बपतिस्मा देने वाले युहन्ना को वे सबसे ऊपर और अपना गुरु मानते और इज्ज़त देते हैं.
वे रेगिस्तान में, ख़ासतौर से, नदियों के क़रीब रहते हैं और सिर्फ दिन के वक़्त ही नहीं, बल्कि रात में भी नहाते-धोते हैं, ताकि अपवित्रता की स्थिति में परमेश्वर की निगाह में गुनाहगार न बन सकें. ”
विद्वानों की राय में, मांडियन की मस्बुता के ज़रिए पवित्र होने/रहने की ख़ास अवधारणा कालांतर में यहूदियों तक पहुंची और वे मिकवाह के नाम से इसका अभ्यास करने लगे.
यहूदी और बपतिस्मा
मांडियन की तरह ही यहूदी भी बपतिस्मा को पवित्रता का पैमाना मानते हैं.इनके धर्मशास्त्रो में इसे मिकवाह के नाम से जाना जाता है.यहूदी यह रस्म शुद्धिकरण के एक अनुष्ठान के रूप में निभाते हैं.ख़ासतौर से, धर्मांतरण के मौक़े पर यानि जब कोई व्यक्ति अपना धर्म छोड़कर यूदावाद (Judaism) क़बूल करता है, तब उसे यहूदी पुजारी/रब्बी द्वारा बपतिस्मा दिया जाता है.
शव के संपर्क में आने पर जैसे अंत्येष्टि आदि में शामिल होने के बाद यहूदी अपवित्र (मूसा के नियमों के अनुसार) समझे जाते हैं, और उन्हें मिकवाह के बाद ही मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति मिलती है.
विशेष मौक़ों के अलावा वीर्य के सामान्य उत्सर्जन चाहे यौन गतिविधि से या रात में उत्सर्जन जैसे स्वप्नदोष या अन्य कारणों से उत्सर्जन की स्थिति में और माहवारी के बाद औरतों के शुद्धिकरण में भी उनके नियमों (तौरात) के अनुसार मिकवे (मिकवाह का स्थान, नहाने की जगह) में स्नान करना ज़रूरी है.
 |
| पुराने और नए ज़माने के मिकवे |
यहूदी मान्यता के अनुसार, एक मिकवे को प्राकृतिक झरने या कुदरती रूप में पाए जाने वाले पानी के स्रोत जैसे कुएं, नदियों या झीलों से जोड़ा जाना ज़रूरी होता है.
यहूदी समुदाय के लिए एक मिकवे का अस्तित्व इतना अहम होता है कि उन्हें आराधनालय बनाने से पहले एक मिकवे का निर्माण करना ज़रूरी होता है.साथ ही, मिकवे के निर्माण कार्य में अगर धन की कमी पेश आए, तो धन जुटाने के लिए टोरा स्क्रॉल और यहां तक कि एक सिनेगॉग की भूमि अथवा भवन भी बेच डालने को कहा गया है.
ईसाई और बपतिस्मा
ईसाईयत में बपतिस्मा की शुरुआत ईसा मसीह के साथ ही हुई.एक यहूदी के रूप में स्वयं ईसा मसीह का भी परंपरा के अनुसार बपतिस्मा हुआ था, जिसे बाद में उन्होंने अपने धर्मप्रचार में भी महत्त्व दिया.इसी कारण उनके अनुयायी भी बपतिस्मा लेने लगे, जो आज भी विभिन्न रूप में जारी है.
बाइबल के अनुसार, ईश्वर ने यर्दन (जॉर्डन) नदी के तट पर रहने वाले बपतिस्मा-दाता युहन्ना (John the Baptist) को यीशु के प्रथम आगमन की घोषणा के लिए चुना था.वे यहूदियों के पाप धोने अथवा प्रायश्चित के लिए उन्हें पानी से बपतिस्मा देते थे.उन्होंने ही यीशु और उनके साथियों को बपतिस्मा दिया.
ईसा मसीह द्वारा बपतिस्मा लिए जाने के बारे में मत्ती अपने सुसमाचारों में आयत 3:16 में कहता है-
” बपतिस्मा लेने के बाद यीशु फ़ौरन पानी में से ऊपर आया.तब आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की पवित्र शक्ति को एक कबूतर के रूप में उस पर (ख़ुद पर) उतरते देखा. ”
ईसाई विद्वानों के अनुसार, बाइबल यह साफ़-साफ़ बताती है कि यहोवा की सेवा करने के इच्छुक लोगों (ईसाई मज़हब अपनाने वालों अथवा इसके अनुयायियों) के लिए बपतिस्मा अति आवश्यक है.मत्ती के सुसमाचारों में आयत 28:19 में यीशु का संदेश इस प्रकार है-
” इसलिए जाओ और सभी राष्ट्रों के लोगों (पूरी दुनिया के लोगों) को मेरा चेला बनना सिखाओ और उन्हें पिता, बेटे और पवित्र शक्ति के नाम से बपतिस्मा दो. ”
दरअसल, ईसाईयत में बपतिस्मा जल के इस्तेमाल के साथ किया जाने वाला एक ऐसा धार्मिक रिवाज/रस्म है, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को चर्च की सदस्यता मिल जाती है.ईसाई बपतिस्मा-दाता इसे धर्मांतरित होकर आए लोगों को अपने मज़हब में शामिल करते समय देते हैं.इसके अलावा, वे अपने अनुयायियों को शुद्दिकरण/प्रायश्चित करने, नामकरण व दत्तक ग्रहण (गोद लेने) के मौक़े पर और टोने-टोटके, झाड़-फूंक आदि जैसे भूत भगाने के लिए भी बपतिस्मा देते हैं.
अधिकांश ईसाई लोगों में ‘पिता के, पुत्र के और पवित्र आत्मा के नाम पर’ बपतिस्मा लेने का रिवाज है.लेकिन कुछ लोग सिर्फ ईसा मसीह के नाम पर भी बपतिस्मा लेते हैं.
ईसाई बपतिस्मा में भी बपतिस्माधारी को गहरे पानी में डुबोने/निमज्जन या आंशिक रूप से डुबोने की की सलाह दी गई है.मगर पुरातात्विक प्रमाणों और चित्रों में लोगों को सामान्य रूप से पानी में खड़ा कर शरीर के उपरी हिस्से पर पानी छिड़कने की रस्म का पता चलता है.
बदलते दौर में आमतौर पर अब, लोगों को बाथटब में बिठाकर या फिर माथे पर सिर्फ तीन बार पानी छिड़ककर (ख़ासतौर से धर्मांतरण के मौक़ों पर) भी बपतिस्मा की रस्म पूरी कर ली जाती है.
इस प्रकार, मांडियन लोगों के मज़हब (Mandaeanism) से मस्बुता के नाम से निकली शुद्दिकरण की रस्म को यहूदियों ने थोड़े बदलाव के साथ मिकवाह के नाम से अपनी मान्यताओं में शामिल किया.फिर, यहूदी मज़हब से निकली ईसाईयत ने भी इसे अपने मातृ-धर्म के रिवाज के रूप में अपना लिया.
नमाज़ की पद्धति
संस्कृत के नम् धातु के नमस् (नमस् शब्द, जो सबसे पहले ऋग्वेद में प्रयोग हुआ है और जिसका अर्थ है आदर और भक्ति में झुक जाना) से निकला फ़ारसी शब्द नमाज़ अरबी में सलात का पर्यायवाची है.सलात शब्द कुरान शरीफ़ में बार-बार आया है, लेकिन दुनिया के अधिकांश हिस्सों में नमाज़ शब्द का ही प्रचलन है.इसे दिन में पांच अदा करने का विधान है.
इतिहास को खंगालें तो पारसी धर्म और इस्लाम में नमाज़ की अवधारणा से पहले भी मांडियन-सबियन धर्मशास्त्रों में अपने ईश्वर को पांच वक़्त पूजने का ज़िक्र मिलता है.
मांडियन और नमाज़
एकेश्वरवादी और ज्ञानवादी धर्म मांडेवाद के अनुयायी जिन्हें मांडियन अथवा सबियन कहा जाता है, एडम, एबेल, सेठ, एनोस, नूह, शेम, राम (अराम) और खासतौर से जॉन द बैप्टिस्ट को अपना नबी (पैगंबर) मानते हैं.मांडव्यवाद (Mandaeanism) अथवा सब्यवाद (Sabianism) के उद्भव काल को लेकर मतभेद है.कुछ विद्वान इसे पहली तीन शताब्दियों ईसवी पूर्व (सी. ई) का बताते हैं, जबकि दूसरे, इसे ईसा पूर्व (बी. सी. ई) और इब्राहिमी पंथ की उत्पत्ति से पहले अस्तित्व में रहे ज़रथोस्ती पंथ यानि पारसी मज़हब से भी पहले या उसके समकालीन होने का दावा करते हैं.मांडियन के विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में प्रमुख, सबसे लंबा एवं प्रसिद्ध गिंज़ा रब्बा में नमाज़ से काफ़ी मिलती-जुलती पूजा-उपासना की चर्चा मिलती है.
गिंज़ा रब्बा का लेखक आदम अथवा उसका बेटा सेथ है, जिससे मिलता-जुलता नाम सीथ का ज़िक्र इस्लामिक पाठ में भी है.
कुरान और हदीसों में सबियन की चर्चा देखने को मिलती है.ख़ासतौर से, कुरान में सबियन का तीन बार उल्लेख हुआ है-
1. वास्तव में विश्वासियों, यहूदियों, ईसाइयों और सबियों, जो कोई भी वास्तव में अल्लाह और अंतिम दिन में यक़ीन रखता है और अच्छा करता है, उनके भगवान के साथ उनका इनाम होगा.उनके लिए कोई डर नहीं होगा, न ही वे शोक करेंगें.(कुरान 2:62)
2. वास्तव में, विश्वासियों, यहूदियों, सबियों और ईसाइयों, जो वास्तव में अल्लाह और अंतिम दिन में यक़ीन रखते हैं और अच्छा करते हैं, उनके लिए कोई डर नहीं होगा, न ही वे शोक करेंगें.(कुरान 5:69)
3. वास्तव में, विश्वासी, यहूदी, सबियन, ईसाई, मैगी और बहुदेववादी (जो अल्लाह से जुड़े हैं) (1) + (2) = उन सभी के बीच वह (अल्लाह) जजमेंट डे पर जज करेगा.यक़ीनन, अल्लाह सभी चीज़ों पर एक गवाह है.(कुरान २२:17)
बुक ऑफ़ आदम कही जाने वाली गिंज़ा रब्बा के गिंज़ा यानि बल/ताक़त और रब्बा यानि ऊपरवाला को मिलाकर इसे ‘ऊपरवाले की ताक़त’ बताया जाता है.दो भागों में बंटे कुल 21 किताबों वाले इस ग्रंथ में शामिल सबसे पहली किताब अल-तौहीद में मून गॉड (सबसे पहले हिन्दू शास्त्रों में वर्णित सोम/चंद्रदेव, रात और वनस्पति के देवता, दिकपाल) को अल्हई कहा है और इस्लाम में वर्णित अल्लाह, रहमान, रहीम की तरह ही इसे ‘हमेशा जीवित रहने वाला’ और सर्वशक्तिमान बताते हुए सिर्फ़ इसी (एकमात्र ईश्वर के रूप में) को मानने पर ज़ोर दिया गया है.इसे ‘सुप्रीम किंग ऑफ़ लाइट’ यानि प्रकाश का सर्वोच्च देवता/शासक बताया गया है.
दुनियाभर में विद्वानों के बीच ये चर्चा और बहस का विषय है कि अल्लाह शब्द क्या चंद्रमा देवता के रूप में उत्पन्न हुआ है, जो पूर्व-इस्लामिक अरब में पूजा जाता था.
अल्लाह शब्द का मूल दरअसल, अरबी भाषा का अल इलाह है.उर्दू और फारसी में अल्लाह को ख़ुदा भी कहा जाता है.
कुछ विद्वानों के मुताबिक़, अल्लाह शब्द का मूल अरामीक अथवा मांडिक भाषा का शब्द इलाहा है.
उल्लेखनीय है कि इस्लाम से पांच सदी पहले की सफ़ा की इमारतों पर हल्लाह शब्द खुदा होता था.छह सदी पहले की ईसाइयों की इमारतों पर भी यह शब्द खुदे होने के प्रमाण मिलते हैं.
इस्लाम से पहले भी अरब में लोग अल्लाह शब्द जानते थे.मक्का की विभिन्न मूर्तियों में एक मूर्ति अल्लाह की भी थी, जिसकी कुरैश कबीले में विशेष मान्यता थी.इसका सम्मान सबसे ज़्यादा था और सृष्टिकार्य इसी से संबंधित समझा जाता था.लेकिन, इसकी शक्तियों और कार्यों को लेकर अरबों में दृष्टिकोण समान नहीं था.कालांतर में, इस्लाम के आगमन के बाद बदलाव आया.
बहरहाल, मांडियन लोगों की भाषा मांडिक अथवा मेंडेइक (Mandaic) अरबी से काफ़ी मिलती-जुलती है.इनके और मुसलमानों के लिबास, दाढ़ी और पगड़ी के अलावा वज़ू और नमाज़ में भी समानता है.गिंज़ा रब्बा में पांच बार की उपासना अथवा नमाज़ की चर्चा है.
 |
| गिंज़ा रब्बा में पांच वक़्त प्रार्थना का ज़िक्र |
रौशनी का सर्वोच्च देवता यानि मांडियन का ईश्वर अल्हई आदम और हौव्वा के बेटे सेथ से कहता है-
” आदम और हौव्वा को रौशनी के सवोच्च देवता, उसकी ताक़त और उसकी महानता का ज्ञान दो.उन्हें सर्वोच्च सत्ता की अनश्वरता और असीमितता के बारे में परिचित कराओ, ताकि बुराई और शैतान उन्हें कभी परेशान न कर सकें.
आदम और हौव्वा को बताओ कि वे ऊपरवाले को दिन में तीन वक़्त और रात में दो वक़्त पूजें. ”
ग़ौरतलब है कि मांडियन धर्मशास्त्रों से प्राप्त विवरण से यहां शैतान के बारे में भी जानकारी मिलती है, जिसका इस्लाम में कई जगहों पर ज़िक्र है.ख़ासतौर से, ये साफ़ हो जाता है कि नमाज़ की अवधारणा इस्लाम में कोई नई नहीं, बल्कि यह तो इस्लाम के आगमन से सैकड़ों सालों पहले से चली आ रही मांडेवाद की पूजा पद्दति और उसके अभ्यास का हिस्सा रही है.
पारसी धर्म और नमाज़
पारसी या फ़ारसी धर्म (Zoroastrianism) दुनिया का बहुत पुराना पैगंबरवादी धर्म है.इसकी स्थापना आर्यों की ईरानी शाखा के एक संत जुराद्रथ/ज़रथुष्ट्र ने की थी.परंपरागत रूप में इसका समय 6000 ईसवी पूर्व का समझा जाता है.इतिहास में, सिकंदर की 330 ईसा पूर्व में विजय से 258 साल पहले 588 ईसा पूर्व इस धर्म का उत्कर्ष काल बताया जाता है.ज़ोरास्ट्रियन अथवा ज़रथोस्ती लोगों का धर्मग्रन्थ अवेस्ता या जेंद अवेस्ता ऋग्वैदिक संस्कृत की ही एक पुरातन शाखा अवेस्ता अथवा अवेस्ताई भाषा में लिखित है.इसमें नमाज़ का उल्लेख है, जो संस्कृत के नमस् शब्द से बना है.फ़ारसी में नमाज़ अरबी के सलात शब्द का पर्यायवाची समझा जाता है.
जानकारों की राय में, पैगंबर ज़रथुष्ट्र के ज़रथुष्ट्रवाद से पहले पारस (पर्शा लोगों का देश जिसे पश्चिम के लोग फ़ारस कहते थे और अरब के नए मुसलमानों की चढ़ाई और क़ब्ज़े के बाद से उसे ईरान के नाम से जानते हैं) देश भी एक सनातन हिन्दू धर्म को मानने वाला देश था.पर्शा लोग भारत के लोगों की तरह ही कई देवी-देवताओं की पूजा करते थे.लेकिन, बाद में आर्यों के स्पीत्मा कुटुंब के पौरुषहस्य और दुधधोवा (दोग्दों) के पुत्र जुराद्रथ (ज़रथुष्ट्र) एक नई विचारधारा लेकर आए और उन्होंने केवल एक ईश्वर अहुर मज़्दा को मानने और उसी को पूजने की शिक्षा दी.
अहुरमज़्दा दरअसल, बुद्धि के देवता समझे जाते हैं और हिन्दुओं के वरुण देवता से बहुत मिलते-जुलते हैं.मगर, वास्तव में ज़रथुष्ट्र और उनके अहूर मज़्दा के उद्भव के साथ ही दुनिया में पहली बार एक पैगंबर और एकेश्वरवादी धर्म को स्थान मिला.ज़न्नत और दोज़ख़ (स्वर्ग और नरक) तथा स्पेन्ता मेन्यु या स्पेन्ता अमेशा के रूप में अच्छाई का देवता और अंगिरा मेन्यु या अहीरमान के रूप में शैतान का प्रादुर्भाव हुआ.त्याग-तपस्या, परीक्षा और कष्टकारी अभ्यासों से परे यह नई व्यवस्थावादी विचारधारा दुनिया को लुभाने लगी.
विद्वानों के अनुसार, ज़ोरोएस्ट्रियन युगांतशास्त्र और दानव विज्ञान की प्रमुख अवधारणाओं ने अब्रह्मिक धर्मों को प्रभावित किया.ख़ासतौर से, इनका इस्लाम पर कितना असर हुआ, यह पारसी और इस्लाम में चिन्वत और अल-सीरत के अध्ययन से स्पष्ट पता चलता है.
जॉन विल्सन ने अपनी किताब ‘The Parsi Religion’ (पेज संख्या 381) में पारसी धर्म के आधारभूत पहलुओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से दी है.
दुनियाभर में महज़ 1 लाख नब्बे हज़ार की संख्या (न्यू यॉर्क टाइम्स की २००६ में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक़) में बचे ज़ोरास्ट्रियन या पारसी लोगों का धर्म (ज़रथोस्ती धर्म) कभी पारस अथवा फ़ारस (ईरान) का राजधर्म और दुनिया का एक ताक़तवर धर्म था.यह वही काल था जब राजा सुदास का आर्यावर्त में शासन था और दूसरी ओर हज़रत इब्राहीम अपना धर्मप्रचार कर रहे थे.इस दौरान, वे ज़रथुष्ट्र के उपदेशों में अहुर मज़्दा संबंधी एकेश्वरवादी बातों से वे प्रभावित हुए.विद्वानों के अनुसार, फ़ारसी मज़हब में स्वर्ग और नरक का अस्तित्व और वहां जाने से पहले हर आत्मा को न्याय के दिन का सामना करने जैसी अवधारणाएं कालांतर में ईसाई और इस्लाम ने भी आत्मसात कर ली.नमाज़ भी इन्हीं में से एक है.
इस्लाम में नमाज़
दुनिया के दूसरे धर्मों की अपनी उपासना पद्धति की तरह ही इस्लाम में नमाज़ का काफ़ी महत्त्व है.इसे मुसलमानों के पांच फ़र्जों में से एक बताया गया है.यह मर्द और औरत, दोनों के लिए समान रूप से ज़रूरी है और ऐसी मान्यता है कि इसे छोड़ने वाले को माफ़ी नहीं मिलती तथा क़ब्र और बरोज़े क़यामत (क़यामत/प्रलय के दिन) में उसका अज़ाब (पाप का दंड, यातना) का शिकार होना तय है.
नमाज़ के लिए अज़ान (पुकार) होती है और मुसलमान अपने सांसारिक कार्यों को छोड़कर ख़ुदा की इबादत के लिए तैयार होते हैं.वे वज़ू कर यानि स्वच्छ होकर, किबले (मक्का) की ओर मुंह कर दुवा पढ़ते हैं, और कुरान शरीफ़ से कुछ तिलावत करते हैं, जिसमें फ़ातिहा (कुरान की पहली सूरा) का पढ़ना ज़रूरी होता है.
इस्लाम में पांच वक़्त की नमाज़ों की मिसाल ऐसी है, मानो ईमान वालों के दरवाज़े पर पांच पवित्र नहरें बह रही हैं.बंदे को उनमें नहाकर अपने सारे मैल-कालिख धो देना है, और कामयाब इंसान बनना है.
ग़ौरतलब है कि दूसरे एकेश्वरवादी-पैगंबरवादी मज़हबों में भी उपासना-पद्धति को लेकर मिलती-जुलती मान्यताएं हैं.इस्लाम की तरह ही कड़े प्रावधान भी हैं.ख़ासतौर से, ज़ोरास्ट्रियन यानि पारसी लोगों की नमाज़-प्रार्थना की व्यवस्था, इसके तौर-तरीक़े आदि इस्लाम में नमाज़ की पद्धति से काफ़ी मिलते-जुलते हैं.इतनी समानता है कि मानो दोनों मज़हबों में बहुत क़रीबी रिश्ता रहा हो, जबकि दोनों के उद्भव-काल और परिस्थितियों में बहुत फ़र्क है.इस विषय पर कई विद्वानों ने शोध किए हैं और अपनी-अपनी राय दी है.
इस बात पर आम राय है कि जिस तरह ज़ोरोएस्ट्रियन के नबी जोरास्टर ने ख़ुदा को अहुर मज़्दा कहकर पुकारा और उसे पांच वक़्त पूजने की विधि बताई, जिसे नमाज़ अथवा गेह (Geh Prayer) कहा गया, उसी तरह इस्लाम में अल्लाह की इबादत के लिए सलात लफ्ज़ बेशक़ आया लेकिन, नमाज़ भी जो साथ-साथ चली, वो अब भी बाक़ायदा चली जा रही है.सफ़र जारी है भरोसे की डगर पर.
पैगंबरी मज़हब के रूप में पारसी और इस्लाम, दोनों में पांच वक़्त की इबादत (नमाज़/गेह) और उस दौरान सिर ढंकने का नियम है.साथ ही, इसके समय में भी काफ़ी समानता है.मसलन पारसी मज़हब में हवन की प्रार्थना और इस्लाम में फज़र की नमाज़, दोनों अहले सुबह (सूर्योदय से पहले, स्थानीय समय के अनुसार) होती है.इसी तरह, पारसियों की रैपिथवन की प्रार्थना दोपहर, उजायरिन दोपहर बाद और सूर्यास्त से पहले, एविश्रुथ्रिम सूर्यास्त के बाद और उषाहेन की रात की प्रार्थना है तो, इस्लाम में जुहर की नमाज़ दोपहर, दोपहर बाद (जब सूरज ढ़लने की की दिशा में अग्रसर होता है) और सूर्यास्त से पहले असर, शाम के वक़्त (सूर्यास्त के बाद) मग़रिब और रात को ईशा की नमाज़ पढ़ी जाती है.
तमाम शोध और प्रमाण के बाद अब इस सवाल का ज़वाब मिल गया है कि है कि अलग-अलग कालखंड में अस्तित्व में आए मज़हब अपनी प्रवृत्ति और उद्देश्यों को लेकर तो भिन्न हैं, अलग-अलग दिखाई देते हैं मगर, उनकी उपासना पद्धति, रस्मो-रिवाज में बुनियादी समानताएं क्यों हैं.
उल्लेखनीय है कि इस्लाम को तो अस्तित्व में आए महज़ 1400 साल हुए हैं.इब्राहिमी विचारधारा की बुनियाद (यहूदी/यूदावाद के रूप में) भी 2000 साल पहले पड़ी थी.मगर, इससे भी सैकड़ों-हजारों साल पहले वज़ूद में रहे पंथों-मज़हब में बपतिस्मा और नमाज़ जैसी ही अवधारणा और तरीकों का चलन था.इससे साफ़ है कि इब्राहिमी मज़हब यानि यहूदी, ईसाई और इस्लाम ने पूर्ववर्ती मज़हब-पंथों में प्रचलित मान्यताओं और पूजा-पद्दति को ही थोड़े बदलावों के साथ उनका नाम बदलकर अपना लिया.
बहरहाल, दुनियावी मामलों में अपना स्वार्थ होता है और प्रतियोगिता भी.मगर यहां स्थिति दूसरी है और कॉपीराइट के मामले से उलट यह, अलग-अलग सभ्यता-संस्कृतियों के पूर्वकाल में एक दूसरे के निकट होने के संकेतों के साथ-साथ वर्तमान में भी समरसता का संदेशवाहक है, जिसे गहराई से समझने की ज़रूरत है.
Multiple ads
 सच के लिए सहयोग करें
सच के लिए सहयोग करें 
कई समाचार पत्र-पत्रिकाएं जो पक्षपाती हैं और झूठ फैलाती हैं, साधन-संपन्न हैं. इन्हें देश-विदेश से ढेर सारा धन मिलता है. इनसे संघर्ष में हमारा साथ दें. यथासंभव सहयोग करें


















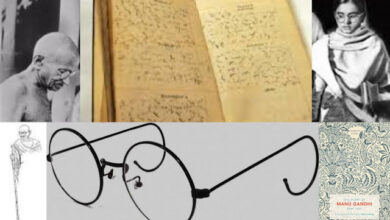

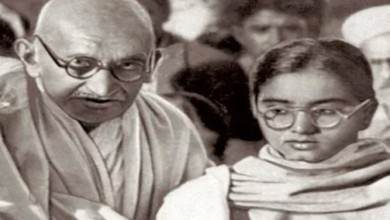
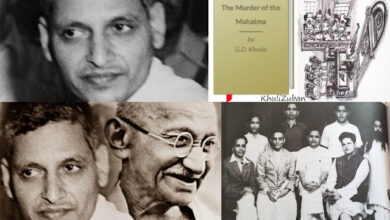

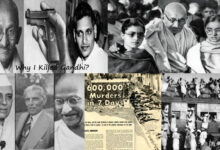
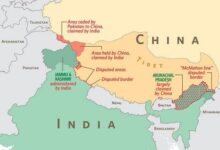
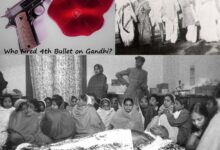
Thank you very much for sharing, I learned a lot from your article. Very cool. Thanks.